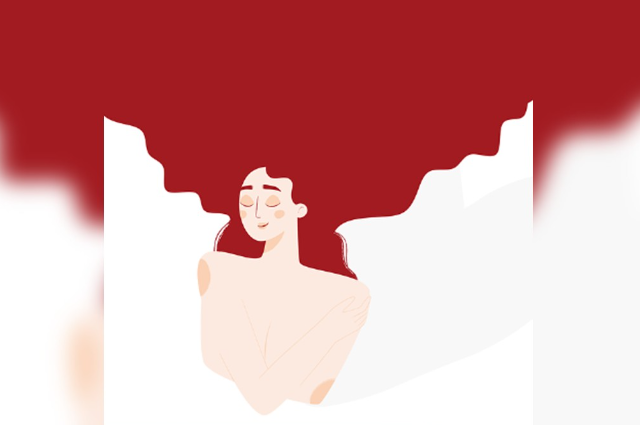
लोग जो अक्सर निकल जाते हैं कोई 'अपना' ढूँढने के लिए—
कभी खुदा को, कभी भगवान को, तो कभी किसी इंसान के लिए।
लोग चाहते हैं ऐसा कुछ ऐसा ढूंढना
जिसके साथ वो खुश रहे,
जो बात अब तक दिल में दफन है
उसे कह सके।
पर जिसकी उन्हें तलाश है
वह कभी उनकी नहीं थी,
वे बस ढूंढ रहे हैं कुछ पराया
"अपना" बनाने के लिए।
लेकिन क्या उन्हें "मैं" मिल गया?
वह मैं—जो बचपन से उनसे जुड़ा हुआ है,
जिसके साथ उन्होंने अपनी हर एक सांस ली है,
जिसके लिए वह कोई 'अपना' ढूंढ रहे हैं।
क्या वह सच में "मैं" की इच्छाओं को जानते हैं?
क्या उन्हें पता है—
यह "मैं" कभी चॉकलेट मिलते ही क्यों हंस देता है,
और क्यों यह "मैं" कभी मिठाई के डिब्बे को देखकर
भी अंदर से रोने लग जाता है?
क्यों यह "मैं" हर दिन एक सा नहीं रहता,
और क्यों इस "मैं" को कोई ढूंढा हुआ 'अपना' चाहिए
बिना यह जाने कि वास्तव में "मैं" को "मैं" से क्या चाहिए।
वे ढूंढ रहे हैं कोई 'अपना' "मैं" के लिए।
"मैं"—जो हमेशा से 'अपना' ही था।
लेकिन क्यों "मैं" को अब भी यह नहीं पता
कि उसे खुश कैसे रहना है?
"मैं" को क्यों यह नहीं पता
कि उसे क्या करना है?
"मैं" को क्यों यह नहीं पता
कि किसी को ढूंढ कर क्या सच में 'अपना' बनाया जा सकता है?
"मैं" बाहरी दुनिया में कोई 'अपना' ढूंढ रहा है,
वो इस उम्मीद में है कि वह 'अपना'
"मैं" को जानने में मदद करेगा।
उस "मैं" को जानने में
जिसे वह अपने साथ पहली सांस से लिए घूम रहा है।
शायद इस "मैं" को नहीं पता
कि जिस अपने की तलाश में वह भटक रहा है,
उसे अपने के पास भी एक "मैं" है—
और वह "मैं" भी कोई 'अपना' ढूंढ रहा है।
क्या "मैं" हमेशा "मैं" ही बना रहेगा,
या कभी किसी के ढूंढने पर
दूसरे का 'अपना' हो जाएगा?
अगर किसी का "मै" मेरा ढूँढ़ा हुआ 'अपना' हो गया
तो क्या वह अपने "मैं" को भूल जाएगा?
क्या वह खुद के "मैं" का ख्याल रख पाएगा?
"मैं"—जो 'अपना' है,
वह 'अपना' जो बचपन से "मैं" है,
क्यों उसे किसी दूसरे का "मैं" नहीं,
बल्कि खुद का ढूंढा हुआ 'अपना' चाहिए।
वह "मैं" जो बचपन से 'अपना' था,
उस "मैं" को खुद ही नहीं पता
कि खुश कैसे रहना है।
क्या वह "मैं" किसी ढूंढते हुए 'अपने' को
खुश रख पाएगा—
जो अपने "मैं" को छोड़कर किसी और के "मैं" का 'अपना' बना है।
और क्या हो अगर "मैं" को कोई ढूंढा 'अपना' नहीं,
बल्कि "मैं" को कोई "मैं" मिले?
