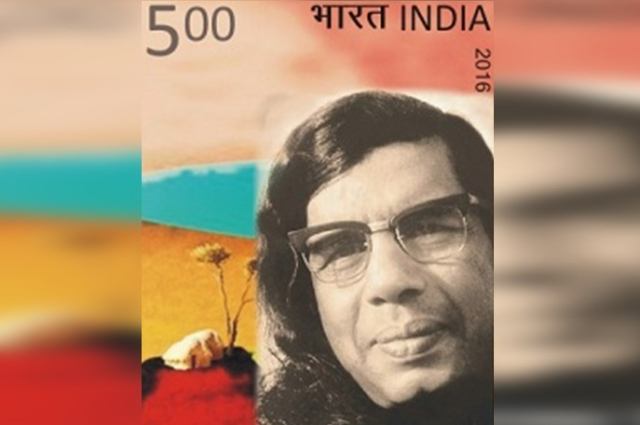फणीश्वर नाथ रेणु हिंदी साहित्य के आंचलिक एवं गहरे लोक-संपृक्त उपन्यासकार तथा कथाकार के रूप में प्रतिष्ठित हैं| लोक संस्कृति की जितनी गहरी पकड़ इनके कथा साहित्य में दिखती है अन्यत्र कहीं दुर्लभ है| ना सिर्फ इनके कथा साहित्य में लोक संस्कृति की झलक है बल्कि इनकी कथा की भित्ति या कहें तो सम्पूर्ण महल ही सुदृढ़, टिकाऊ और मन को छुने वाली लोकभाषा के नींव पर टिकी हुई है| इसमें कोई दो राय नहीं कि जो भाषा पढ़े-लिखे प्रोफेशनल और आधुनिक अंग्रेजी जगत में गवारों और गलीचों की भाषा है, वही भाषा रेणु के कथा साहित्य की भी भाषा है| लेकिन जब इन्हें वाक्यों के साथ रेणु अपने कथा में खपाते हैं तो इनकी कथा किसी क्लासिकल सिनेमा सी आँखों के सामने चलने लगती है| ऐसा लगता है जैसे ‘पहलवान की ढोलक’ का पहलवान कथा में नहीं माथे के भीतर नाच रहा है जिसे हम देख रहे हैं| ऐसा लगता हैं कि रसप्रिया का मोहना आँखों के सामने आम चूस रहा हैं और ठेस का सिरचन..!
अपने उतार-चढ़ाव भरे जीवन में भी रेणु ने सदा ही हिंदी साहित्य को पुष्पित-पल्लवित किया| कहा जाता है कि 1954 में आया इनका उपन्यास ‘मैला आँचल’ ने अपने आंचलिक तेवर से हिंदी साहित्य को नई दिशा दी और आंचलिक साहित्य पर विमर्श इसके पश्चात ही शुरू हुआ| रेणु ने अपने उपन्यास में लोक या कहें तो अंचल को ही नायक बना डाला है वो भी कच्चे और अनगढ़ रूप में| जहाँ एक तरफ शस्य श्यामलता है तो एक तरफ धूल,एक तरफ फूल है तो एक तरफ शूल| इनके साहित्य की विशेषता है अंचल में सजीवता की प्रस्तुति, रेणु जी के प्रस्तुति का ढंग हमारे मन में ऐसा प्रभाव पैदा करता है कि उनके खेत,खलिहान,घास काटती स्त्री,मेड, डोलता अरहर सब सजीव मालूम पड़ने लगता है मानो कोई रिकॉर्डिंग देख रहें हों,फिल्म की तरह एक पर एक शब्द चित्र दौड़ता है| जैसे कोई रेल आँखों के सामने से गुजर रहा हो| इनका रचना संसार लोक संस्कृति का संसार है या यो कहें लोक त्योहारों का साहित्यिक म्युजियम है,जहाँ चलन से गायब हो रहे या हो गए उत्सवों का भी दर्शन किया जा सकता है| रेणु के साहित्य में शहर से भिन्न एक देहाती संस्कृति का एक गवाड़पन है तो चेतना भी है| श्रद्धा है तो संस्कार भी| जो परती से लेकर उर्वर तक फैली हुई है|ये ‘मैला आँचल’ से ‘परती कथा’ तक ऐसे फैला है जैसे धरती पर आकाश| मैंने जब रेणु जी के आँचलिक उपन्यास(यहाँ ध्यातव्य हो कि रेणु जी अपने लिए आँचलिक उपन्यासकार का संबोधन पसंद नहीं करते थे|) ‘मैला आँचल’ के शीर्षक को सुना तो मुझे ये अच्छा नहीं लगा| मैंने सोचा,आँचल मैला क्यों हो भला? आँचल तो साफ़ होना चाहिए! फिर समझते देर ना लगी कि रेणु के शीर्षक का आँचल खेत में धान बोती किसी स्त्री का है या नहीं तो धूर पर धान काटती मोहना की माँ का| जिसने धूल को चूम अपनी धवलता बिसरा/भूला दी है| रेणु के इस शीर्षक को पढ़ कर सुमित्रानंदन पन्त जी की कविता संग्रह ग्राम्या में संकलित भारतमाता का अंश स्मरण हो आता है-
भारत माता ग्रामवासिनी खेतों में फैला है श्यामल धूल भरा मैला सा आँचल मिट्टी की प्रतिमा उदासिनी|1
‘मैला आँचल’ का केन्द्रीय कथ्य पुरे ग्रामांचल का समग्र यथार्थ है जिसमें अंधविश्वास भी है और चेतना भी, चोरी भी है और दान भी, दमन भी है और प्रतिकार भी| साथ ही साथ इसमें लुप्तप्राय आकर्षण को जीवित रखने की क्षमता भी है, इसमें लोकगीत है,लोकभाषा है,नदी-नाले,डबरे,पशु-पक्षी,हल-बैल,मंदिर-मस्जिद,गेहूँ-खेत सबकुछ है|इसमें रेणु ने ग्रामीण जीवन पद्धति का चित्रण भदेस ग्राम्य भाषा और समतुल्य वातावरण के साथ किया है| रेणु की कथाओं में ईश्वरवाद और उत्सव का आद्वितीय उदाहरण दृष्टिगत होता है जो अन्यत्र नहीं|आस्था का हांल ये है कि मैला आँचल में तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद काली थान के सामने आने पर सर पर टोपी रख कर काली माँ को प्रणाम करता है|2 देवी के प्रति ऐसी श्रद्धा भावविह्वल कर देती है| ये रेणु के गाँव में ही संभव है|परती परिकथा में परानपुर गाँव के लोग परती भूमि पर निर्वासित परमा देवता की पूजा करते हैं|क्योकि उनकी ऐसी मान्यता है कि परमा देव सभी की मान्यता पूरी कर सकते हैं|3 बारह-बारह साल के काग बांझों को बच्चा दिया है परमादेव ने| बैजू की बहू को याद है कि आँचल में केला और अमरुद गिरा दूसरे दिन सुबह से ही उसे मिचली आने लगी| गले हुए गोढ़ी करिया सामू को परमादेव के वाक् ने आराम दिया|4
देवता रेणु के ठेठ लोगों के ह्रदय में ऐसे बसे हैं कि वे कोई काम बिना देवता को पूजे प्रारंभ ही नहीं कर सकते| तभी तो ‘मैला आँचल’ में भंडारे से पहले काली धान की पूजा की गई|5 लोक में देवता के प्रति ऐसी आस्था है, ऐसा विश्वास है कि कलिमुद्दीपुर के पास साकुड़ के पेड़ की डाली पर लटकती हुई बाबनदास की खद्दर की ओली के अवशेष लाल डोरी को कोई दुखिया वृद्ध चेथरिया पीर समझकर अपने आँचल का कोई खूँट फाड़कर बांध देती है और मनोकामना पूर्ण होने की आशा करने लगती है|6 ऐसी श्रद्धा और कहाँ दृष्टिगत हो सकती है| रेणु जी का अंचल देवताओं का प्रजनन स्थल है|
यहाँ पीपर,पाकर,आम,जामुन,बरगद, पीपल सभी में मान्यताओं के देवता बसते है| खेलावन सिंह की पत्नी अपने बच्चे का मति सुधारने के लिए पीर बाबा से प्रार्थना करती है|और मनौती पूरी होने पर मादक पदार्थ चढाने की बात कहती है|7 रेणु के लिए कही गई भारत यायावर की ये पंक्तियाँ बिकुल सही ही है कि वे साधारण जन की आत्मा के सजग और मर्मी शिल्पी हैं|अगर वे साधारण जन की आत्मा के शिल्पी ना होते तो ‘बट बाबा’ की कराह को जन –जन के ह्रदय में ना अनुभव करते?वैसे भी बट-बाबा का धराशायी होना कोई आम बात नहीं थी| कैसे होती ये आज से थोड़े ना थे,वर्षों से थे| कितने वर्षों से? ये किसी जीवित को नहीं पता! ये सबों के देवता थे यानी उतने ही हिन्दू के जितने की मुस्लिम के| एकादशी,पूर्णिमा में इनकी फूल,सिन्दूर धूप –दीप से पूजा होती| बट सावित्री में सुहागिनों को आशीष देते उनकी जटाएं इतनी फ़ैल गयी थी जिसे देख लोग हर्षित रहते थे|जब बट बाबा सूखने को हुए तो मनौती मांगने वालों की भीड़ लग गई|श्रद्धा भक्ति की धारा ऐसी तीव्र हो गयी कि कभी पेड़-पत्थर की पूजा ना करने की कसम खाने वाली मंडर की पतोहू भी चार आने का बतासा लेकर बाबा से अपने पति की रिहाई का निवेदन करने चली गयी| लछमिनिया,कलरू महतो, टहलू पासवान,भजू धानुक सब मनौती मांग रहे थे| जब पेड़ गिरा तो गाँव वालों का कलेजा फट गया| मानो गाँव अनाथ हो गया हो|8 एक पेड़ के प्रति ऐसी श्रद्धा ऐसा लगाव,सांस्कृतिक सम्पन्नता, रागात्मकता और कोमलता रेणु की कथाओं में ही संभव है| भारतीय संस्कृति की यहाँ जीवन को उज्जवल बनाने के लिए लौकिक और परलौकिक दोनों तरह की संभावना मौजूद है| त्योहारों के मूल में धार्मिक भावनाएं कैद रहती हैं जहाँ लोग उत्तम भविष्य की कामना देवी-देवता से करते हैं|तभी तो ‘विघटन के क्षण’ में रानीडीह की कुमारी कन्याओं ने रात में भाई के दीर्घायु होने के लिए लाल माटी वाले खेत पर सामा-चकेवा का खेल खेला| सामा,चकवा, खंजन,बटेर,चाहा,पनकौआ,हांस,बनहांस, भेम्हा आदि की पूजा की गयी| सैकड़ों चुगलों के पुतले फूँकें| पुतलों की शिखाएँ जली| अगहनी धान के खेतों में कुछ पांच वर्षों बाद सामा चरा रही है रानीडीह की कुमारियाँ| हवाओं में चुगलों के व्यंगात्मक गीत उड़ रहें है-
“घर-घर में तू झगड़ा लगाबे,बाप बेटा से रगडा कराबे
सब दिन पानी में आग लगाबे, बिन कारन सब दिन छुछुवावे|
तोर टिकी में आगि लगे रे चुगले.... छुछुन्दरमुंह... मूँहझौंसे चुगले|”9
‘तबो एकला चलो रे’ में छठी मैया के प्रति विश्वास ऐसा है कि लोग छठी मैया से कहते हैं कि वे बथान में पाड़ा ना दें और घर में बेटा ही दें|10
रेणु के मैला आँचल में मेरीगंज के लोग सतुआनी पर्व मनाते है|साल के पहले दिन सिरवा पर्व होता है जिसमें चूल्हे नहीं जलते| लोग मानते हैं कि साल भर जलने वाले चूल्हे के लिए ये दिन विश्राम का होता है| होली तो जैसे रेणु के समाज के लिए आवश्यक पर्व में एक है तभी तो रेणु कहते हैं कि जो जिए सो खेले फाग| दुसरे पर्व त्योहारों को टाल भेई दिया जा सकता है लेकिन मादक वासंती फाग को कैसे टाला जा सकता| जब मजराई आम के बाग़ से हवा आकर मतवाला बना जाती है| स्त्रियाँ होली का गीत गाती है –
अरे बहियाँ पकदि झकझोरि श्याम दे
फूटल रेशम जोड़ी चूड़ी,
मसकी गई चोली, भीगावल साडी
आँचल उड़ी जाए हो
ऐसो होरी मचायो श्याम रे|
रेणु के जुलूस में ईद और दुर्गापूजा गाँव के हिन्दू और मुसलमान दोनों सामान रूप से मनाते हैं| सौहार्द कायम है |ऐसा ही ‘रोमांस शुन्य प्रेमकथा’ में देखने को मिलता है|
लोक जीवन में आज भी त्योहार प्रचलित है लेकिन उनके पीछे की धार्मिक भावना का ह्रास हुआ है| नई पीढ़ी में पर्वों के प्रति उत्साह कम हुआ है| ये कोई तुरंत हुआ है ऐसा नहीं है बल्कि रेणु के समय में भी युवा पर्वों से विमुख थे| उनकी नजरों में पर्व रूढिगत समाज की बेवकूफी के उदाहरण हैं, जिसे बंद करना चाहिए| आज के परिवर्तनकारी समय में जब संस्कृति अपने अस्तित्व को अक्षुण रखने के लिए डटी है, वहां रेणु का साहित्य संसार उनका संबल बनकर खड़ा है| तभी तो रेणु संस्कार और संस्कृति के साहित्यकार के रूप में शिखर पर हैं और रहेंगे|
. . .
सन्दर्भ:
- सुमित्रानंदन पंत: ग्राम्या,लोकभारती प्रकाशन,इलाहाबाद,1977, पेज न.45
- फणीश्वरनाथ रेणु: मैला आँचल, राजकमल प्रकाशन,दिल्ली,2008,पृष्ठ-10
- फणीश्वरनाथ रेणु, परती: परिकथा,राजकमल प्रकाशन,दिल्ली,2007,पृष्ठ-93
- फणीश्वरनाथ रेणु, परती: परिकथा ,पृष्ठ-94
- रेणु: मैला आंचल,पृष्ठ-41
- रेणु: मैला आंचल,पृष्ठ-304
- रेणु: मैला आंचल,पृष्ठ-254
- फनीश्वरनाथ रेणु: बट बाबा, मेरी कथा यात्रा,इन्द्रप्रस्थ प्रकाशन,दिल्ली,2012,
पृष्ठ-(15-19) - फनीश्वरनाथ रेणु: विघटन के क्षण, चुनी हुई कहानियाँ, वाणी प्रकाशन,दिल्ली,
पृष्ठ -294 - वही: तबे एकला चलो रे, पृष्ठ -165